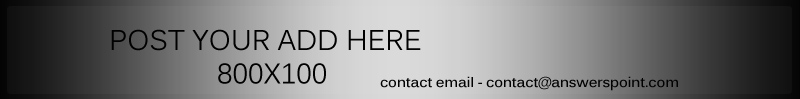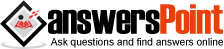आधी रात में (Aadhi Raat Mein) - रबीन्द्रनाथ टैगोर
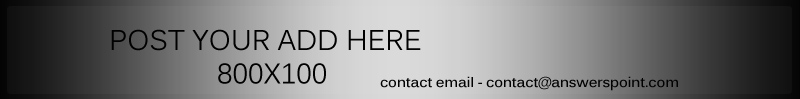
आधी रात में (Aadhi Raat Mein)
-: रबीन्द्रनाथ टैगोर :-
‘‘डॉक्टर! डॉक्टर!!’’
‘‘परेशान कर डाला! इतनी रात गए–’’
आँखें खोलकर देखा, अपने दक्षिणाचरण बाबू थे। हड़बड़ाकर उठकर टूटी पीठ की चौकी घसीटकर उन्हें बैठने को दी और उद्विग्न भाव से मुँह की ओर देखा। घड़ी देखी, रात के ढाई बजे थे।
दक्षिणाचरण बाबू ने विवर्ण मुख विस्फारित नेत्रों से कहा, ‘‘आज रात को फिर वही उपद्रव मच गया है–तुम्हारी औषधि कुछ काम नहीं आई।’’
मैंने कुछ संकोच के साथ कहा, ‘‘मालूम होता है, आपने शराब की मात्रा फिर बढ़ा दी है।’’
दक्षिणाचरण बाबू ने अत्यंत खीझकर कहा, ‘‘यह तुम्हारा भारी भ्रम है। शराब की बात नहीं; आद्योपांत विवरण सुने बिना तुम असली कारण का अनुमान नहीं कर पाओगे।’’
आले में मिट्टी के तेल की छोटी-सी ढिबरी मंद-मंद जल रही थी, मैंने उसे उकसा दिया; प्रकाश थोड़ा जगमगा उठा और बहुत-सा धुआँ निकलने लगा। धोती का छोर देह के ऊपर खींचकर अखबार बिछे चीड़ के खोखे पर बैठ गया। दक्षिणाचरण बाबू कहने लगे–‘‘मेरी पत्नी जैसी गृहिणी मिलना बड़ा कठिन है। किंतु तब मेरी अवस्था ज्यादा नहीं थी, सहज ही रसाधिक्य हो गया था, तिस पर काव्य-शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया था, इससे निरे गृहिणीपन से मन नहीं भर पाता था।
कालिदास का यह श्लोक प्रायः मन में उभर आता–
गृहिणी सचिवः सखी मिथः
प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ।
किंतु मेरी पत्नी पर ललित कलाविधि का कोई उपदेश नहीं चल पाता था और यदि सखीभाव से प्रथम-संभाषण करता तो वे हँसकर उड़ा देतीं। गंगा के प्रवाह से जिस प्रकार इंद्र का ऐरावत परास्त हो गया था वैसे ही उनकी हँसी के सामने बड़े-बड़े काव्यों के टुकड़े और प्यार के अच्छे-अच्छे संभाषण क्षण-भर में ही खिसककर बह जाते। हँसने की उनमें अपूर्व क्षमता थी।
उसके बाद, आज लगभग चार बरस हुए मुझे भयंकर रोग ने धर दबाया। होंठों पर दाने निकल आए। ज्वर-विकार हुआ, मरने की-सी हालत हो गई। बचने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी जवाब दे गया। तभी मेरे एक आत्मीय ने कहीं से एक ब्रह्मचारी को ला उपस्थित किया; उसने गाय के घी के साथ एक जड़ी पीसकर मुझे खिला दी। चाहे औषधि के गुण से हो या भाग्य के फेर से, उस बार मैं बच गया।
बीमारी के समय मेरी स्त्री ने दिन-रात एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। उन कई एक दिनों में एक अबला स्त्री ने मनुष्य की सामान्य शक्ति के सहारे प्राणपण से व्याकुलता के साथ द्वार पर आए हुए यमदूतों से अनवरत युद्ध किया। अपने संपूर्ण प्रेम, समस्त हृदय, सारी सेवा से उसने मेरे इस अयोग्य प्राण को स्वयं मानो दुधमुँहें शिशु समान दोनों हाथों से छिपाकर ढक लिया था। आहार नहीं, नींद नहीं, संसार में और किसी का कोई ध्यान न रहा।
यम तो पराजित बाघ के समान मुझे अपने चंगुल से छोड़कर चले गए, किंतु जाते-जाते मेरी स्त्री पर एक प्रबल पंजा मार गए।
मेरी स्त्री उस समय गर्भवती थीं, कुछ समय बाद उन्होंने एक मृत संतान को जन्म दिया। उसके साथ से ही उनके नाना प्रकार के जटिल रोगों का सूत्रपात हुआ। तब मैंने उनकी सेवा आरंभ कर दी। उससे वे बहुत व्याकुल हो उठीं। कहने लगीं, ‘‘अरे! क्या करते हो? लोग क्या कहेंगे! इस प्रकार दिन-रात तुम मेरे कमरे में मत आया-जाया करो।’’
स्वयं पंखे की हवा के बहाने यदि रात को ज्वर के समय मैं पंखा झलने चला जाता तो भारी छीना-झपटी मच जाती। किसी दिन उनकी शुश्रूषा के कारण यदि मेरे नियमित भोजन के समय में दस मिनट की देर हो जाती, वह भी नाना प्रकार का अनुनय, अनुयोग का कारण बन जाती। थोड़ी-सी सेवा करने पर लाभ के बदले हानि होने लगती। वे कहतीं, ‘‘पुरुषों का इतना अति करना अच्छा नहीं है।’’
हमारे बरानगर के उस घर को, मेरा ख्याल है तुमने देखा है। घर के सामने ही बगीचा है और बगीचे के सामने गंगा बहती है। हमारे सोने के कमरे के नीचे ही दक्षिण की ओर मेहँदी की बाड़ लगाकर कुछ जमीन घेरकर मेरी पत्नी ने अपने मनपसंद बगीचे का एक टुकड़ा तैयार किया था। संपूर्ण बगीचे में वही भाग अत्यंत सीधा-सादा और एकदम देशी था। अर्थात् उसमें गंध की अपेक्षा वर्ण की बहार, फूल की तुलना में पत्तों का वैचित्र्य नहीं था, और गमलों में लगाए छोटे पौधों के समीप कमची के सहारे कागज की बनी लैटिन में लिखे नाम की जय-ध्वजा नहीं उड़ती थी। बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, कनेर और रजनीगंधा का ही प्रादुर्भाव कुछ अधिक था। एक विशाल मौलश्री वृक्ष के नीचे सफेद संगमरमर पत्थर का चबूतरा बना था। स्वस्थ रहने पर वे स्वयं खड़ी होकर दोनों समय उसको धोकर साफ करवाती थीं। ग्रीष्मकाल में काम से छुट्टी पाने पर संध्या समय वही उनके बैठने का स्थान था। वहाँ से गंगा दिखती थीं, किंतु गंगा से कोठी की छोटी नौका में बैठे बाबू लोग उनको नहीं देख पाते थे।
बहुत दिन तक चारपाई पर पड़े-पड़े एक दिन चैत्र में शुक्लपक्ष की संध्या को उन्होंने कहा, ‘‘घर में बंद रहने से मेरा प्राण न जाने कैसा हो रहा है आज एक बार अपने उस बगीचे में जाकर बैठूँगी।’’
मैंने उनको बहुत सँभालकर पकड़े हुए धीरे-धीरे ले जाकर उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे बनी पत्थर की वेदी पर लिटा दिया। यों तो मैं अपनी जाँघ पर ही उनका सिर रख सकता था, किंतु मैं जानता था कि वे उसे विचित्र-सा आचरण समझेंगी, इसलिए एक तकिया लाकर उनके सिर के नीचे रख दिया।
मौलश्री के दो-एक खिले हुए फूल झर रहे थे। और शाखाओं के बीच से छायांकित ज्योत्स्ना उनके शीर्ण मुख के ऊपर आ पड़ी। चारों ओर शांति और निस्तब्धता थी; उस सघन गंधपूर्ण छायांधकार में एक ओर चुपचाप बैठकर उनके मुख की ओर देखकर मेरी आँखों में पानी भर आया।
मैंने धीरे-धीरे बहुत समीप पहुँचकर अपने हाथों से उनका एक उत्तप्त जीर्ण हाथ ले लिया। इस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ देर इसी प्रकार चुपचाप बैठे-बैठे मेरा हृदय न जाने कैसा उद्वेलित हो उठा! मैं बोल उठा, ‘‘तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूँगा।’’
तभी समझा, इस बात के कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरी पत्नी हँस पड़ी। उस हँसी में लज्जा थी, सुख था और थोड़ा-सा अविश्वास था; और उसमें काफी मात्रा में परिहास की तीव्रता भी थी। प्रतिवादस्वरूप कोई बात न कहकर उन्होंने केवल अपनी उसी हँसी से ही व्यक्त किया, ‘‘किसी दिन भूलोगे नहीं, यह कभी संभव नहीं और मैं इसकी प्रत्याशा भी नहीं करती।’’
इस सुमिष्ट सुतीक्ष्ण हँसी के भय से ही मैंने कभी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह प्रेमालाप करने का साहस नहीं किया। उनके सामने न रहने पर जो अनेक बातें मन में आतीं, उनके सामने जाते ही वे अत्यंत व्यर्थ लगने लगतीं। छत् अक्षरों में जो बातें पढ़ने पर नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगती है उनको मुँह से कहते हमें क्यों हँसी आती है, यह मैं आज तक नहीं समझ सका।
बातचीत में तो वाद-प्रतिवाद चल जाता है, किंतु हँसी के ऊपर तर्क नहीं चलता, इसलिए चुप होकर रह जाना पड़ा। ज्योत्स्ना उज्ज्वलतर हो उठी। एक कोयल बार-बार कुहू-कुहू करती हुई चंचल हो गई। मैं बैठा-बैठा सोचने लगा, ऐसी ज्योत्स्ना-रात्रि में भी क्या पिकवधू बधिर हो गई है?
बहुत चिकित्सा करने पर भी मेरी पत्नी का रोग शांत होने के कोई लक्षण नहीं दिखे। डॉक्टर ने कहा, ‘‘एक बार जलवायु परिवर्तन करके देखना अच्छा होगा।’’
मैं पत्नी को लेकर इलाहाबाद चला गया।
इतना कहकर दक्षिणा बाबू सहसा चौंककर चूप हो गए। संदेहपूर्ण भाव से मेरे मुख की ओर देखा, उसके बाद दोनों हाथों से सिर थामकर सोचने लगे। मैं भी चुप बैठा रहा। ताक में केरोसीन की ढिबरी टिमटिमाकर जलने लगी और निस्तब्ध कमरे में मच्छरों की भिनभिनाहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हठात् मौन तोड़कर दक्षिणा बाबू ने कहना शुरू किया–‘‘वहाँ हारान डॉक्टर पत्नी की चिकित्सा करने लगे।’’
अंत में बहुत दिन तक स्थिति में कोई अंतर होते न देखकर डॉक्टर ने भी कह दिया, मैं भी समझ गया और मेरी पत्नी भी समझ गई कि उनका रोग अच्छा होने वाला नहीं है। उनको सदा रुग्ण रहकर ही जीवन काटना पड़ेगा।
तब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ‘‘जब न तो व्याधि ही दूर होती है और न मरने की ही कोई आशा है तब और कितने दिन इस जीवन्मृत को लिए काटोगे? तुम दूसरा विवाह करो।’’
यह मानो केवल एक युक्तिपूर्ण और समझदारी की बात थी–इसमें कोई भारी महत्त्व, वीरत्व या कुछ असामान्य था, ऐसा लेश-मात्र भी उनका भाव नहीं था।
अब मेरे हँसने की बारी थी। किंतु मुझमें क्या उस प्रकार हँसने की क्षमता है! मैं उपन्यास के प्रधान नायक के समान गंभीर और सगर्व भाव से कहने लगा, ‘‘जितने दिन इस शरीर में प्राण है...’’
वे टोककर बोलीं, ‘‘‘बस-बस, और अधिक मत बोलो! तुम्हारी बात सुनकर तो मैं दंग रग जाती हूँ।’’
पराजय स्वीकार न करते हुए मैं बोला, ‘‘इस जीवन में और किसी से प्रेम नहीं कर सकूँगा।’’
सुनकर मेरी पत्नी जोर से हँस पड़ीं। तब मुझे परास्त होना पड़ा।
मैं नहीं जानता कि उस समय कभी अपने आपसे भी स्पष्ट स्वीकार किया था या नहीं, किंतु इस समय मैं समझ रहा हूँ कि उस आरोग्य-आशाहीन सेवा-कार्य से मैं मन ही थक गया था। उस काम में चूक करूँगा, ऐसी कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी; अतएव, चिर जीवन इस चिररुग्ण को लेकर बिताना होगा, यह कल्पना भी मुझे पीड़ाजनक प्रतीत हुई। यौवन की प्रथम बेला में जब सामने देखा था तब प्रेम की कुहक में, सुख के आश्वासन में, सौंदर्य की मरीचिका में मुझे अपना समस्त भावी जीवन खिलता हुआ दिखाई दिया था, अब आज से लेकर अंत तक केवल आशाहीन सुदीर्घ प्यासी मरुभूमि।
मेरी सेवा में वह आंतरिक थकान उन्होंने अवश्य ही देख ली थी उस समय मैं नहीं जानता था, किंतु अब जरा भी संदेह नहीं है कि वे मुझे संयुक्ताक्षरहीन ‘शिशु शिक्षा’ के प्रथम भाग के समान बहुत ही आसानी से समझ लेती थीं। इसीलिए जब उपन्यास का नायक बनकर मैं गंभीर मुद्रा में उनके पास कवित्व प्रदर्शित करने जाता तो वे बड़े अकृत्रिम स्नेह, किंतु अनिवार्य कौतूक के साथ हँस उठतीं। मेरे अपने अगोचर अंतर की सब बातों को भी वे अंतर्यामी के समान जानती थीं, इस बात को सोचकर आज भी लज्जा से मर जाने की इच्छा होती है।
डॉक्टर हारान हमारे स्वजातीय थे। उनके घर प्रायः मेरा निमंत्रण रहता। कुछ दिनों के आने-जाने के बाद डॉक्टर ने अपनी कन्या के साथ मेरा परिचय करा दिया। कन्या अविवाहित थी, उसकी उम्र पंद्रह की रही होगी। डॉक्टर ने कहा कि उनको मन के अनुकूल पात्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसका विवाह नहीं किया। किंतु बाहर के लोगों से अफवाह सुनता–कन्या के कुल में दोष था।
किंतु, और कोई दोष नहीं था। जैसी सुंदर थी वैसी ही सुशिक्षिता। इस कारण कभी-कभी एकाध दिन उनके साथ नाना विषयों पर आलोचना करते-करते घर लौटते मुझे रात हो जाती, पत्नी की औषधि देने का समय निकल जाता। वे जानती थीं कि मैं डॉक्टर के घर गया हूँ; किंतु उन्होंने एक भी दिन विलंब के कारण के विषय में प्रश्न तक नहीं किया।
मरुभूमि में फिर एक बार मरीचिका दिखाई देने लगी। तृष्णा जब गले तक आ गई थी तभी आँखों के सामने लबालब स्वच्छ जल कलकल, छलछल करने लगा! इस स्थिति में मन को प्राणपण से रोकने पर भी मोड़ नहीं सका।
रोगी का कमरा मुझे पहले से दुगना निरानंद लगने लगा। तब सेवा करने और औषधि खिलाने का नियम सब प्रायः भंग होने लगा।
डॉक्टर हारान बीच-बीच में मुझसे प्रायः कहते रहते, जिनका रोग अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है उनका मरना ही भला है, क्योंकि जीवित रहने से उनको स्वयं भी सुख नहीं मिलता, और दूसरों को भी दुख होता है।’’ साधारण रूप से ऐसी बात कहने में कोई दोष नहीं तथापि मेरी स्त्री को लक्ष्य करके इस प्रकार के प्रसंग का उठाना उनके लिए उचित न था। किंतु, मनुष्य के जीवन-मरण के विषय में डॉक्टरों के मन ऐसे अनुभूतिशून्य होते हैं कि वे ठीक प्रकार से हमारे मन की हालत नहीं समझ सकते।
सहसा एक दिन बगल के कमरे से सुना, मेरी पत्नी हारान बाबू से कह रही थीं, ‘‘डॉक्टर, फिजूल में इतनी औषधियाँ खिला-खिलाकर औषधालय का कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? जब मेरी जान ही एक लाइलाज बीमारी है तब कोई ऐसी दवा दो कि यह जान ही निकल जाए और जान छूटे।’’
डॉक्टर ने कहा, ‘‘छिः! ऐसी बातें न करें।’’
यह सुनकर मेरे हृदय को एकबारगी बड़ा आघात पहुँचा। डॉक्टर के चले जाने पर मैं अपनी स्त्री के कमरे में जाकर उनकी चारपाई के सिरहाने बैठ गया, उनके माथे पर धीरे-धीरे हाथ फेरने लगा। वे बोलीं, ‘‘यह कमरा बड़ा गरम है, तुम बाहर जाओ। टहलने जाने का समय हो गया है। थोड़ा टहले बिना रात को तुम्हें भूख नहीं लगेगी।’’
टहलने जाने का अर्थ था, डॉक्टर के घर जाना। मैंने उनको समझाया था कि भूख लगने के लिए थोड़ा टहल लेना विशेष आवश्यक है। आज मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ, वे प्रतिदिन की मेरी इस छलना को समझती थीं। मैं ही निर्बोध था जो सोचता था कि ये निर्बोध हैं।
यह कहकर दक्षिणाचरण बाबू हथेली पर सिर टिकाए बहुत देर तक मौन बैठे रहे। अंत में बोले, ‘‘मुझे एक गिलास पानी ला दो!’’ पानी पीकर कहने लगे–एक दिन डॉक्टर बाबू की पुत्री मनोरमा ने मेरी पत्नी को देखने के लिए आने की इच्छा प्रकट की। पता नहीं क्यों, उनका यह प्रस्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। किंतु प्रतिवाद करने का कोई कारण नहीं था। वे एक दिन संध्या को मेरे घर आ उपस्थित हुईं।
उस दिन मेरी पत्नी की पीड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ बढ़ गई थी। जिस दिन उनका कष्ट बढ़ता उस दिन वे अत्यंत स्थिर और चुपचाप रहतीं; केवल बीच-बीच में मुट्ठियाँ बँध जातीं और मुँह नीला हो जाता, इसी से उनकी पीड़ा का अनुमान होता। कमरे में कोई आहट नहीं थी, मैं बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा था। उस दिन टहलने जाने का मुझसे अनुरोध करें, इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं थी या हो सकता है, मन ही मन उनकी यह इच्छा रही हो कि अत्यधिक कष्ट के समय मैं उनके पास रहूँ। चौंध न लगे, इससे केरोसिन की बत्ती दरवाजे के पास थी। कमरा अँधेरा और निस्तब्ध था। केवल कभी-कभी पीड़ा के समय कुछ शांत होने पर मेरी पत्नी का दीर्घ निःश्वास सुनाई पड़ता था।
इस समय मनोरमा कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उलटी ओर से बत्ती का प्रकाश आकर मुख पर पड़ा। प्रकाश से चौंधिया जाने के मारे कमरे में कुछ भी न देख पाने के कारण वे कुछ क्षणों तक दरवाजे के पास खड़ी इधर-उधर करने लगीं।
मेरी स्त्री ने चौंककर मेरा हाथ पकड़कर पूछा, ‘‘वह कौन है?’’ अपनी उस दुर्बल अवस्था में सहसा अपरिचित व्यक्ति को देखकर उन्होंने डरकर मुझसे दो-तीन बार अस्पष्ट स्वर में प्रश्न किया, ‘‘कौन है? वह कौन है जी?’’
न जाने मेरी कैसी दुर्बुद्धि हुई कि मैंने पहले ही कह दिया, ‘‘मैं नहीं जानता।’’ कहते ही मानो किसी ने मुझे चाबुक मारा। दूसरे क्षण मैं बोला, ‘‘ओह, अपने डॉक्टर बाबू की लड़की!’’
पत्नी ने एक बार मेरे मुख की ओर देखा, मैं उनके मुख की ओर नहीं देख सका। दूसरे ही क्षण उन्होंने क्षीण स्वर में अभ्यागत से कहा, ‘‘आप आइए!’’ मुझसे बोलीं, ‘‘उजाला करो।’’
मनोरमा कमरे में आकर बैठ गईं। उनके साथ मरीज की थोड़ी-बहुत बातचीत चलने लगी। इसी समय डॉक्टर बाबू आ उपस्थित हुए।
वे अपने औषधालय से दो शीशी औषधि साथ ले आए थे। उन शीशियों को बाहर निकालते हुए वे मेरी पत्नी से बोले, ‘‘यह नीली शीशी मालिश करने के लिए और यह खाने के लिए। देखिए, दोनों को मिलाइएगा नहीं, यह औषधि भयंकर विष है।’’
मुझे भी एक बार सावधान करते हुए दोनों दवाइयों को चारपाई के पास मेज पर रख दिया। विदा लेते समय डॉक्टर ने अपनी पुत्री को बुलाया।
मनोरमा ने कहा, ‘‘पिताजी, मैं यहाँ रह जाऊँ? साथ में कोई महिला नहीं है, उनकी सेवा कौन करेगा?’’
मेरी स्त्री व्याकुल हो उठीं। बोलीं, ‘‘नहीं-नहीं, आप कष्ट न कीजिए! पुरानी नौकरानी है, वह माँ की भाँति मेरी सेवा करती है।’’
डॉक्टर हँसते हुए बोले, ‘‘ये लक्ष्मीस्वरूपा हैं! चिरकाल से दूसरे की सेवा करती आ रही हैं, दूसरे की सेवा सहन नहीं कर सकतीं।’’
पुत्री को लेकर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय मेरी स्त्री बोली, ‘‘डॉक्टर बाबू, ये इस बंद कमरे में बहुत समय से बैठे हैं, इनको थोड़ी देर बाहर घुमा ला सकते हैं?’’
डॉक्टर बाबू ने मुझसे कहा, ‘‘चलिए न, आपको नदी के किनारे थोड़ा घुमा लाएँ।’’
मैं तनिक आपत्ति प्रकट करने के बाद शीघ्र ही राजी हो गया। डॉक्टर बाबू ने चलते समय दवाइयों की दोनों शीशियों के संबंध में फिर मेरी पत्नी को सावधान कर दिया।
उस दिन मैंने डॉक्टर के घर ही भोजन किया। लौटने में रात हो गई। आकर देखा, मेरी स्त्री छटपटा रही थीं। मैंने पश्चात्ताप से पीड़ित होकर पूछा, ‘‘क्या तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई है?’’
वे उत्तर न दे सकीं। चुपचाप मेरे मुख की ओर देखने लगीं। उस समय उनका गला रुँध गया था।
मैं तुरंत रात में ही डॉक्टर को बुला लाया।
डॉक्टर आकर पहले तो बहुत देर तक कुछ समझ ही न सके। अंत में उन्होंने पूछा, ‘‘क्या तकलीफ बढ़ गई है? एक बार दवा की मालिश करके क्यों न देखा जाए।’’
यह कहते हुए उन्होंने टेबल से शीशी उठाकर देखी, वह खाली थी।
मेरी पत्नी से पूछा, ‘‘क्या आपने गलती से यह दवा खाई है?’’
मेरी पत्नी ने गर्दन हिलाकर चुपचाप बताया, ‘‘हाँ।’’
डॉक्टर तुरंत अपने घर से पंप लाने के लिए गाड़ी में दौड़े। मैं अर्ध-मूर्च्छित-सा पत्नी के बिस्तर पर पड़ गया।
उस समय, जिस प्रकार माता पीड़ित शिशु को सांत्वना देती है उसी प्रकार उन्होंने मेरे सिर को अपने वक्षस्थल के पास खींचकर हाथों के स्पर्श द्वारा मुझे अपने मन की बात समझाने की चेष्टा की। केवल अपने उस करुण स्पर्श के द्वारा ही वे मुझसे बार-बार कहने लगीं, ‘‘दुखी मत होना, अच्छा ही हुआ। तुम सुखी रहोगे, यही सोचकर मैं सुख से मर रही हूँ।’’
जब डॉक्टर लौटे तो जीवन के साथ-साथ मेरी स्त्री यंत्रणाओं का भी अवसान हो गया था।
दक्षिणाचरण फिर से एक बार पानी पीकर बोले, ‘‘ओह! बड़ी गरमी है!’’ यह कहते हुए तेजी से बाहर निकलकर बरामदे में दो-चार बार टहलने के बाद फिर आ बैठे। अच्छी तरह स्पष्ट हो गया, वे कहना नहीं चाहते थे, किंतु मानो मैंने जादू से उनसे बात निकलवा ली हो। फिर आरंभ किया–
मनोरमा से विवाह करके घर लौट आया।
मनोरमा ने अपने पिता की सम्मति के अनुसार मुझसे विवाह किया। किंतु जब मैं उससे प्रेम की बात कहता, प्रेमालाप करके उसके हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करता तो वह हँसती नहीं, गंभीर बनी रहती। उसके मन में कहाँ किस जगह क्या खटका लग गया था, मैं कैसे समझता?
इन्हीं दिनों मेरी शराब पीने की लत बहुत बढ़ गई।
एक दिन शरद् के आरंभ में संध्या को मनोरमा के साथ अपने बरानगर के बाग में टहल रहा था। घोर अंधकार हो आया था। घोंसलों में पक्षियों के पंख फड़फड़ाने तक की आहट नहीं थी, केवल घूमने के रास्ते के दोनों किनारे घनी छाया से ढँके झाऊ के पेड़ हवा में सर-सर करते काँप रहे थे।
थकान का अनुभव करती हुई मनोरमा उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे शुभ्र पत्थर की वेदी पर आकर अपने हाथों के ऊपर सिर रखकर लेट गई। मैं भी पास आकर बैठ गया।
वहाँ और भी घना अंधकार था; आकाश का जो भाग दिखाई दे रहा था, वह पूरी तरह तारों से भरा था। वृक्षों के तले के झींगुरों की ध्वनि मानो अनंत गगन के वक्ष से च्युत निःशब्दता पर ध्वनि की एक पतली किनारी बुन रही हो।
उस दिन भी शाम को मैंने कुछ शराब पी थी, मन खूब तरलावस्था में था। अंधकार जब आँखों को सहन हो गया तब वृक्षों की छाया के नीचे पांडु वर्ण वाली उस शिथिल-आँचल श्रांतकाय रमणी की अस्पष्ट मूर्ति ने मेरे मन में एक अनिवार्य आवेग का संचार कर दिया। मुझे लगा, वह मानो कोई छाया हो, मैं उसे मानो किसी भी तरह अपनी बाँहों में बाँध नहीं सकूँगा।
इसी समय अँधेरे झाऊ वृक्षों की चोटियों पर जैसे आग जल उठी हो; उसके पश्चात् कृष्ण पक्ष के क्षीण हरिद्रावर्ण चाँद ने धीरे-धीरे वृक्षों के ऊपर आकाश में आरोहण किया। सफेद पत्थर पर सफेद साड़ी पहने उसी थकी लेटी रमणी के मुख पर ज्योत्स्ना आकर पड़ी। मैं और न सह सका। पास आकर हाथों में उसका हाथ लेकर बोला, ‘‘मनोरमा, तुम मेरा विश्वास नहीं करतीं, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता।’’
बात कहते ही मैं चौंक उठा। याद आया, ठीक यही बात मैंने कभी किसी और से भी कही थी। और तभी मौलश्री की शाखाओं के ऊपर होती हुई झाऊ वृक्ष की चोटी पर से होती हुई कृष्ण पक्ष के पीतवर्ण खंडित चाँद के नीचे से, गंगा के पूर्वी किनारे से लेकर गंगा के सुदूर पश्चिमी किनारे तक हा-हा-हा-हा-हा-हा करतीं एक हँसी अत्यंत तीव्र वेग से प्रवाहित हो उठी। वह मर्मभेदी हँसी थी या अभ्रभेदी हाहाकार था, कह नहीं सकता। मैं उसी क्षण मूर्च्छित होकर पत्थर की वेदी से नीचे गिर पड़ा।
मूर्च्छा भंग होने पर देखा, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हूँ। पत्नी ने पूछा, ‘‘तुम्हें अचानक यह क्या हुआ?’’
मैंने काँपते हुए कहा, ‘‘तुमने सुना नहीं, समस्त आकाश को परिपूर्ण करती हुई एक हा-हा करती हँसी ध्वनित हुई थी?’’
पत्नी ने हँसकर कहा, ‘‘वह हँसी थोड़े ही थी। पंक्ति बाँधकर पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ा था, उन्हीं के पंखों का शब्द सुनाई दिया था। तुम इतने से ही डर जाते हो?’’
दिन के समय मैं स्पष्ट समझ गया कि वह सचमुच पक्षियों के झुंड के उड़ने का ही शब्द था। इस ऋतु में उत्तर दिशा में हंस-श्रेणी नदी के कछार में चारा चुगने के लिए आती है, किंतु संध्या हो जाने पर यह विश्वास टिक नहीं पाता था। उस समय लगता, मानो चारों ओर समस्त अंधकार को भरती हुई सघन हँसी जमा हो गई हो, किसी सामान्य बहाने से ही अचानक आकाशव्यापी अंधकार को विदीर्ण करके ध्वनित हो उठेगी। अंत में ऐसा हुआ कि संध्या के बाद मनोरमा से मुझे कोई भी बात कहने का साहस न होता।
तब मैं बरानगर के अपने घर को त्यागकर मनोरमा को साथ लेकर नौका पर बाहर निकल पड़ा। अगहन के महीने में नदी की हवा से सारा भय भाग गया। कुछ दिनों बड़े सुख में रहा। चारों ओर के सौंदर्य से आकर्षित होकर–मनोरमा भी मानो बहुत दिन बाद मेरे लिए अपने हृदय का रुद्ध धीरे-धीरे खोलने लगी।
गंगा पार कर, खड़ पार कर अंत में हम पद्मा में आ पहुँचे। भयकारी पद्मा उस समय हेमंत ऋतु की विवरलीन भुजंगिनी के समान कृश निर्जीव-सी लंबी शीतनिद्रा में मग्न थी। और दक्षिण के ऊँचे किनारे पर गाँवों के आमों के बगीचे इस राक्षसी नदी के मुख में करवट बदलती और विदीर्ण तट-भूमि छपाक से टूट-टूटकर गिर पड़ती। यहाँ घूमने की सुविधा देखकर नौका बाँध दी।
एक दिन घूमते हुए हम दोनों बदुत दूर चले गए। सूर्यास्त की स्वर्णच्छाया विलीन होते ही शुक्ल पक्ष का निर्मल चंद्रालोक देखते-देखते खिल उठा। अंतहीन शुभ्र बालू के कछार पर जब अजस्त्र, मुक्त उच्छ्वसित ज्योत्स्ना एकदम आकाश की सीमाओं तक प्रसारित हो गई तब लगा मानो जन-शून्य चंद्रालोक के असीम स्वप्न-राज्य में केवल हम दो व्यक्ति ही भ्रमण कर रहे हों। एक लाल शॉल मनोरमा के सिर से उतरता उसके मुख को वेष्टित करते हुए उसके शरीर को ढँके हुए था। निस्तब्धता जब गहरी हो गई, केवल सीमाहीन, दिशाहीन शुभ्रता और शून्यता के अतिरिक्त जब और कुछ भी न रहा तब मनोरमा ने धीरे-धीरे हाथ बढ़ाकर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अत्यंत पास आकर वह मानो अपना संपूर्ण तन-मन-जीवन-यौवन मेरे ऊपर डालकर एकदम निर्भय होकर खड़ी हो गई। मैंने पुलकित-उद्वेलित हृदय से सोचा, कमरे के भीतर क्या भला यथेष्ट प्रेम किया जा सकता है? यदि ऐसा अनावृत मुक्त अनंत आकाश न हो तो क्या कहीं दो व्यक्ति बँध सकते हैं? उस समय लगा–हमारे न घर है, न द्वार है, न कहीं लौटना है। बस हम इसी प्रकार हाथ में हाथ लिए अगम्य मार्ग में उद्देश्यहीन भ्रमण करते हुए चंद्रालोकित शून्यता पर पैर धरते मुक्त भाव से चलते रहेंगे।
इसी प्रकार चलते-चलते एक जगह पहुँचकर देखा, थोड़ी दूर पर बालुका-राशि के बीच एक जलाशय-सा बन गया है, पद्मा के उतर जाने पर उसमें पानी जमा रह गया था।
उस मरु बालुकावेष्टित निस्तरंग, गाढ़ निद्रामग्न, निश्चल जल पर विस्तृत ज्योत्स्ना की रेखा मूर्च्छित भाव से पड़ी थी। उसी स्थान पर आकर हम दोनों व्यक्ति खड़े हो गए–मनोरमा ने न जाने क्या सोचकर मेरे मुख की ओर देखा, अचानक उसके सिर पर से शॉल खिसक गया। मैंने ज्योत्स्ना से खिला हुआ उसका वह मुँह उठाकर चूम लिया।
उसी समय उस जनमानव-शून्य निःसंग मरुभूमि के गंभीर स्वर में न जाने कौन तीन बार बोल उठा, ‘‘कौन है? कौन है?’’
मैं चौंक पड़ा, मेरी पत्नी भी काँप उठी। किंतु दूसरे ही क्षण हम दोनों ही समझ गए कि यह शब्द मनुष्य का नहीं था, अमानवीय भी नहीं था। कछार में विहार करने वाले जलचर पक्षी की आवाज थी। इतनी रात को अचानक अपने निरापद निभृत निवास के समीप जन-समागम देखकर वह चौंक उठा था।
भय से चौंककर हम दोनों झटपट नौका में लौट आए। रात को आकर बिस्तर पर लेट गए। थकी होने के कारण मनोरमा शीघ्र ही सो गई। उस समय अंधकार में न जाने कौन मेरी मसहरी के पास खड़ा होकर सुषुप्त मनोरमा की ओर एक लंबी जीर्ण अस्थि-पिंजर-मात्र अँगुली दिखाकर मानो मेरे कान में बिलकुल चुपचाप अस्फुट स्वर में बारंबार पूछने लगी, ‘‘कौन है? कौन है? वह कौन है जी?’’
झटपट उठकर दियासलाई धिसकर बत्ती जलाई। उसी क्षण वह छायमूर्ति विलीन हो गई। मेरी मसहरी को कँपाकर, नौका को डगमगाकर, मेरे स्वेद-सने शरीर के रक्त को वर्ष करके हा-हा-हा-हा-हा-हा करती हुई एक हँसी अंधकार रात्रि में बहती हुई चली गई। पद्मा को पार कर, पद्मा के कछार को पार कर, उसके तटवर्ती समस्त सुप्त देश, ग्राम, नगर पार कर मानो वह चिरकाल से देश-देशांतर, लोक-लोकांतर को पार करती क्रमशः क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम होकर सुदूर की ओर चली जा रही थी, धीरे-धीरे वह मानो जन्म-मृत्यु के देश को पीछे गई, क्रमशः वह मानो सुई के अग्रभाग के समान क्षीणतम हो आई। मैंने इतना क्षीण स्वर पहले कभी नहीं सुना, कल्पना भी नहीं की, मानो मेरे दिमाग में अनंत आकाश हो और वह शब्द कितनी ही दूर क्यों न जा रहा हो, किसी भी प्रकार मेरे मस्तिष्क की सीमा छोड़ नहीं पा रहा हो। अंत में जब नितांत असह्य हो गया तब सोचा, बत्ती बुझाए बिना सो नहीं पाऊँगा। जैसे ही रोशनी बुझाकर लेटा वैसे ही मेरी मसहरी के पास, मेरे कान के समीप, अँधेरे में वह अवरुद्ध स्वर फिर बोल उठा, ‘‘कौन है? कौन है? वह कौन है जी?’’ मेरे हृदय का रक्त भी उसी पर ताल देता हुआ क्रमशः ध्वनित होने लगा, ‘‘कौन है? कौन है? वह कौन है जी?’’ ‘‘कौन है? कौन है? वह कौन है जी?’’ उसी गहरी रात में निस्तब्ध नौका में मेरी गोलाकार घड़ी भी सजीव होकर अपनी घंटे की सुई को मनोरमा की ओर घुमाकर शेल्फ के ऊपर से ताल मिलाकर बोलने लगी, ‘‘कौन है? वह कौन है जी? कौन है? कौन है? वह कौन है जी?’’
कहते-कहते दक्षिणा बाबू का रंग फीका पड़ गया उनका गला रुँध आया। मैंने उनको सहारा देते हुए कहा, ‘‘थोड़ा पानी पीजिए!’’ इसी समय सहसा मेरी केरोसीन की बत्ती लुप-लुप करती बुझ गई। अचानक देखा, बाहर प्रकाश हो गया है। कौआ बोल उठा। दहिंगल पक्षी सिसकारी भरने लगा। मेरे घर के सामने वाले रास्ते पर भैंसागाड़ी का चरमर-चरमर शब्द होने लगा। दक्षिणा बाबू के मुख की मुद्रा अब बिलकुल बदल गई।
अब भय का कोई चिह्न न रहा। रात्रि की कुहक में काल्पनिक शंका की मत्तता में मुझसे जो इतनी बातें कह डालीं उसके लिए वे अत्यंत लज्जित और मेरे ऊपर मन ही मन क्रोधित हो उठे। शिष्टाचार-प्रदर्शन शब्द के बिना ही वे अकस्मात उठकर द्रुतगति से चले गए।
उसी दिन आधी रात में फिर मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई, “डॉक्टर! डॉक्टर!”
Hindi Kahani
Rabindranath Tagore ki Rachnaye
- asked 3 years ago
- B Butts